श्री के. राजारमन, आईएएस
डीसीसी के अध्यक्ष और सचिव,
दूसरा तल, संचार भवन, 20, अशोक रोड,
नई दिल्ली, पिन- 110001
विश्व में लगातार बढ़ती परस्पर संबद्धता में भारत एक प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी प्रगति और क्षमता के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वास्तव में भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का आंकड़ा लगभग 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 350 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। दूरसंचार के इस असाधारण विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है जोकि डिजिटल अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान दे रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री का अंत्योदय या समावेश का दृष्टिकोण तब तक संभव नहीं है जब तक हम 'सभी के लिए कनेक्टिविटी' के माध्यम से डिजिटल समावेशन पर काम नहीं करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इस बढ़ोतरी के पूर्ण लाभों का वहन कर सके इसके लिए हमें एक मजबूत और सर्वव्यापी दूरसंचार अवसंरचना और सेवा पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था का भुगतान न केवल अधिकतम हो, बल्कि क्षेत्रों और आबादी के सभी वर्गों में भी व्याप्त हो। जून 2017 आईसीआरआईईआर के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में इंटरनेट के उपयोग में 10% की वृद्धि से हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 3.3% की वृद्धि हो सकती है। ऐसा मूलत: इसलिए है क्योंकि इंटरनेट अन्य भौतिक अवसंरचना की कमी को दूर करता है और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं के अभिगम को सक्षम बना सकता है।
भारत में दूरसंचार क्षेत्र सतत और उचित विकास के लिए ठोस आधार प्रदान करने के लिए तैयार है। भारत में वॉयस डेटा लगभग मुफ्त हो गया है और यह डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। डिवाइस भी तेजी से किफायती होते जा रहे हैं। वास्तव में मोबाइल फोन विभिन्न सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम को सक्षम करने वाले सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रहा है और इंटरनेट अर्थव्यवस्था में 40% योगदान मोबाइल का है। हाल के दिनों में भारत में डेटा की वृद्धि दर लगभग 500% रही है जो न केवल सबसे तेज है, बल्कि दुनिया में भारत को अमेरिका और चीन से आगे मोबाइल डेटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता बना रही है।
नागरिकों, उद्योग और सरकार सहित सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अगले दो वर्षों में लगभग 60 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र में कुल निवेश लगभग 140 बिलियन अमरीकी डालर रहा है जो अपने आप में एक चुनौती बनता जा रहा है। इस प्रकार अपेक्षित स्तर के निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए एक अनुकूल वाणिज्यिक वातावरण का सृजन महत्वपूर्ण है।
दूरसंचार विभाग दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए एक समर्थ कारक की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी सहायक होगा। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) - 2018 विभिन्न कारकों का समग्र दृष्टिकोण अपनाती है जो भविष्य में इस क्षेत्र में सुदृढ़ और गतिशील वृद्धि को सक्षम करते हैं। एनडीसीपी 2018 में जिन प्रमुख विषयों पर विचार किया गया है, उनमें क्षेत्र को प्रभावित करने वाले नियामक और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, स्पेक्ट्रम नीतियां, सभी के लिए कनेक्टिविटी, सेवाओं की गुणवत्ता (क्यूओएस), ईज ऑफ डूईंग बिजनेस और 5जी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) सहित नई प्रौद्योगिकियों का आमेलन शामिल है। 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' दोनों का ही उद्देश्य उपरोक्त सभी कारकों से आगे जाना है।
विभाग सार्वभौमिक मोबाइल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से 'सभी के लिए कनेक्टिविटी' के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की दिशा में कार्य कर रहा है। भारतनेट परियोजना का उद्देश्य लगभग संपूर्ण ग्रामीण आबादी करने के लिए उच्च गति ब्रॉडबैंड अवसंरचना का निर्माण करना है और यह निरंतर इस उद्देश्य हेतु प्रयासरत है। विभिन्न अन्य यूएसओएफ कार्यक्रम भी पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु सेवा से वंचित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहे हैं।
हम वास्तव में आज भारतीय दूरसंचार क्रांति के एक अत्यंत रोमांचक चरण में हैं। हाल ही में संपन्न हुई 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद 5जी सेवाओं की शुरुआत होना प्रमुख उपलब्धि है। हम इस वर्ष यूएसओएफ आरएंडडी फंड लॉन्च करने की उम्मीद करते हैं ताकि नई और सस्ती प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में कार्यनीतियों और अन्य घरेलू फर्मों को सक्षम किया जा सके। मुझे विश्वास है कि डिजिटल समावेश, सभी के लिए कनेक्टिविटी और दूरसंचार क्षेत्र को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने पर नए सिरे से ध्यान देने से हमें जल्द ही उचित और समान विकास के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
डीसीसी के अध्यक्ष और सचिव








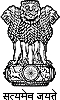 दूरसंचार विभाग
दूरसंचार विभाग




